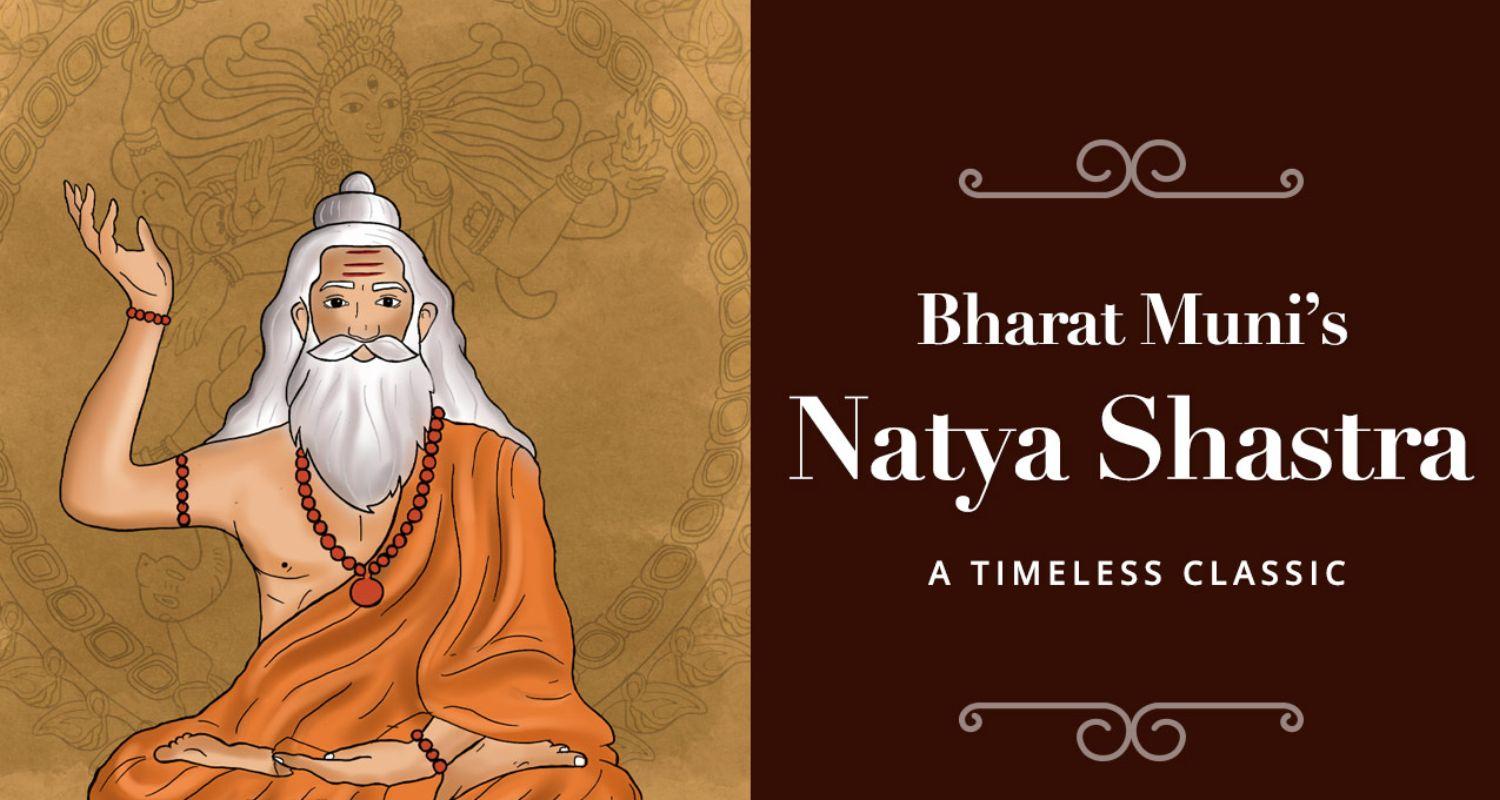‘नाट्यशास्त्र’ को मिली वैश्विक मान्यता, कला जगत के लिए साबित हो रहा कालातीत धरोहर
युनेस्को ने भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर में किया शामिल
पटना।
भारतीय कला और संस्कृति की अमूल्य धरोहर नाट्यशास्त्र को वैश्विक मान्यता मिली है। हाल ही में यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ (MoW) कार्यक्रम के तहत 74 नए अभिलेखों के साथ नाट्यशास्त्र और भगवद्गीता के पांडुलिपियों को इस सूची में शामिल किया गया। पुणे स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संरक्षित इन पांडुलिपियों को “विश्व महत्व और सार्वभौमिक मूल्य” के अंतर्गत संरक्षण हेतु चुना गया है।
जहां भगवद्गीता जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आधार रही है, वहीं नाट्यशास्त्र भारतीय कला, सौंदर्यबोध और अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ओडिशी और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना, पद्म विभूषण डॉ. सोनल मानसिंह के अनुसार, “नाट्यशास्त्र जैसा समग्र कला-ग्रंथ विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है, जो कला के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को इस गहनता से परिभाषित करता हो।”
नाट्यशास्त्र बनाम अरस्तू की ‘पोएटिक्स’
करीब 2500 वर्ष पूर्व रचित नाट्यशास्त्र, भरत मुनि द्वारा संस्कृत में लिखित 36 अध्यायों और 6000 से अधिक श्लोकों का एक विश्वकोशीय ग्रंथ है। अक्सर इसे केवल नृत्य से जोड़कर देखा जाता है, परंतु यह नृत्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला, वेशभूषा, मंच-सज्जा, यहां तक कि संगीत वाद्य निर्माण की प्रक्रियाओं तक का वैज्ञानिक विवेचन करता है।
वहीं दूसरी ओर, विश्वभर में प्रसिद्ध अरस्तू की पोएटिक्स मात्र पाँच अध्यायों में नाटक और कॉमेडी तक सीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार, “पोएटिक्स तो नाट्यशास्त्र का एक अंश मात्र है।”
भाव और रस की सूक्ष्म व्याख्या
नाट्यशास्त्र के सातवें अध्याय ‘भाव अध्याय’ में 49 भावों के माध्यम से 500 से अधिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया है। भरत मुनि ने कला के माध्यम से जीवन के दुख-दर्द से मुक्ति दिलाने और धर्मसम्मत आनंद उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया है।
‘रससूत्र’—यानी कला का सार—के सिद्धांत के अनुसार, सृजनात्मक कार्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि दर्शक के भीतर नैतिक और आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए होना चाहिए।
विश्वभर में नाट्यशास्त्र की उपस्थिति
भारत में विभिन्न क्षेत्रों के अलावा थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में भी नाट्यशास्त्र की परंपराएँ जीवित हैं। थाई कलाकार भरत मुनि के मुखौटे की पूजा कर प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं, जबकि कंबोडिया में यह आज भी एक जीवंत परंपरा है।
काश्मीर के महान विद्वान अभिनवगुप्त द्वारा रचित हजार वर्ष पुराना ग्रंथ अभिनवभारती नाट्यशास्त्र पर सबसे प्रामाणिक टीका माना जाता है, जिसमें रस-सिद्धांत और आत्मानुभूति के गहरे संबंधों को उकेरा गया है।
आधुनिक कला में नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता
नाट्यशास्त्र में वर्णित मूल्यांकन उपकरण आज भी किसी भी कला रूप का आकलन करने के लिए प्रासंगिक हैं, चाहे वह विश्व के किसी भी भूभाग से संबंधित हो। प्रसिद्ध चित्रकार अकबर पदमसी ने भी नाट्यशास्त्र के वर्णित रंग-सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान के रंग-सिद्धांत से मेल खाता हुआ बताया था।
विशेषज्ञों का मानना है कि नाट्यशास्त्र की वैश्विक मान्यता से न केवल भारतीय कलाकारों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि विश्वभर के कलाकार भी कला को सामाजिक और आत्मिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित कर सकेंगे।